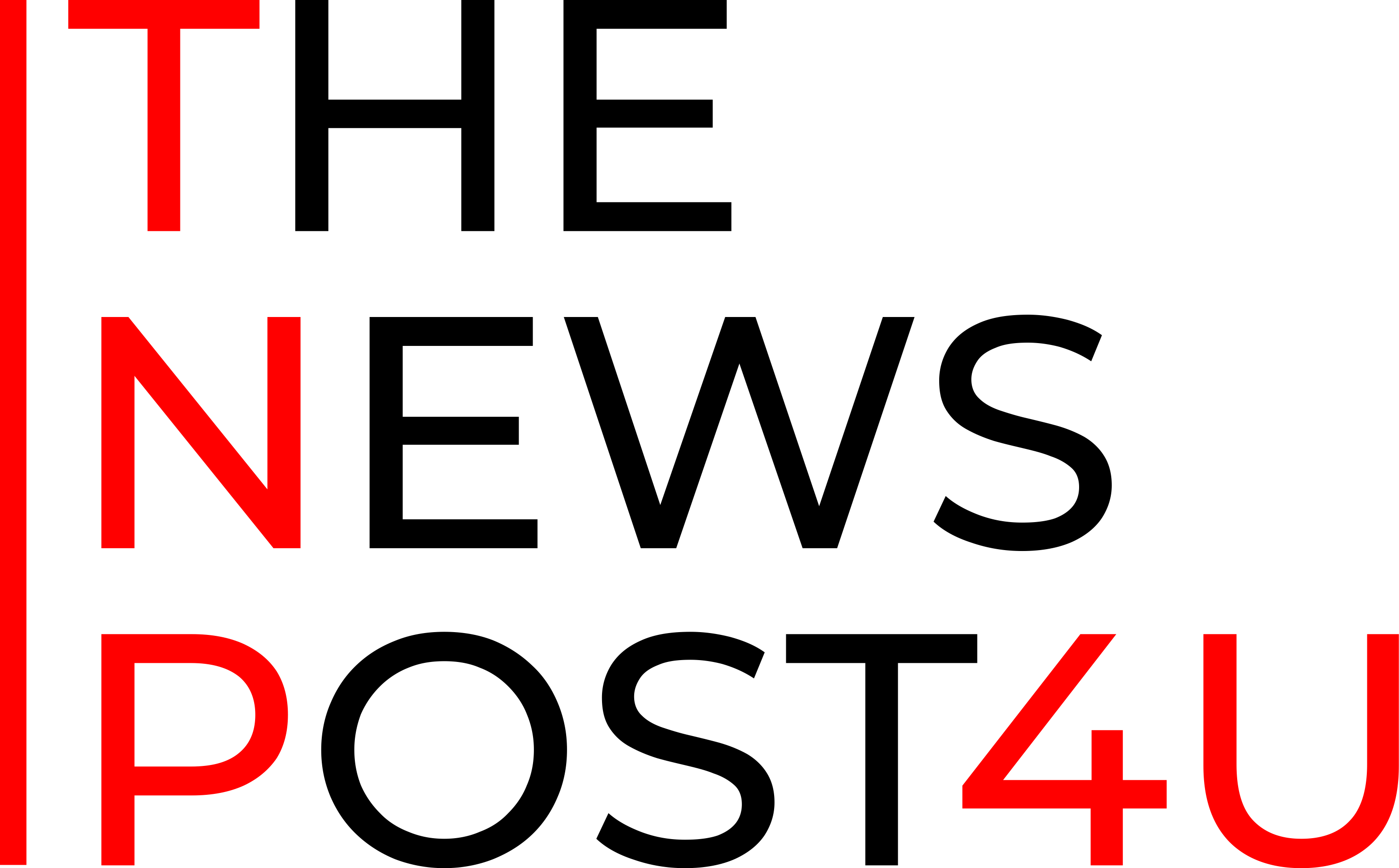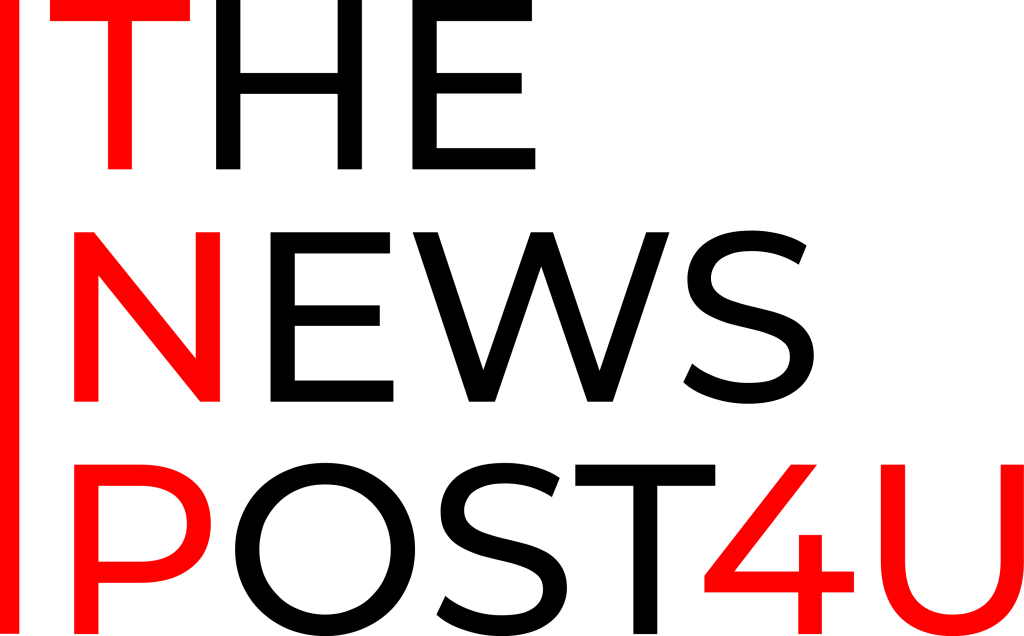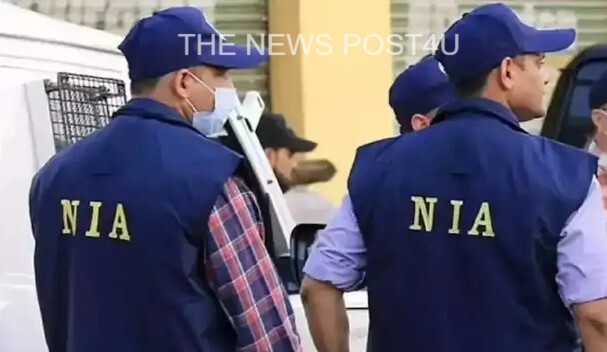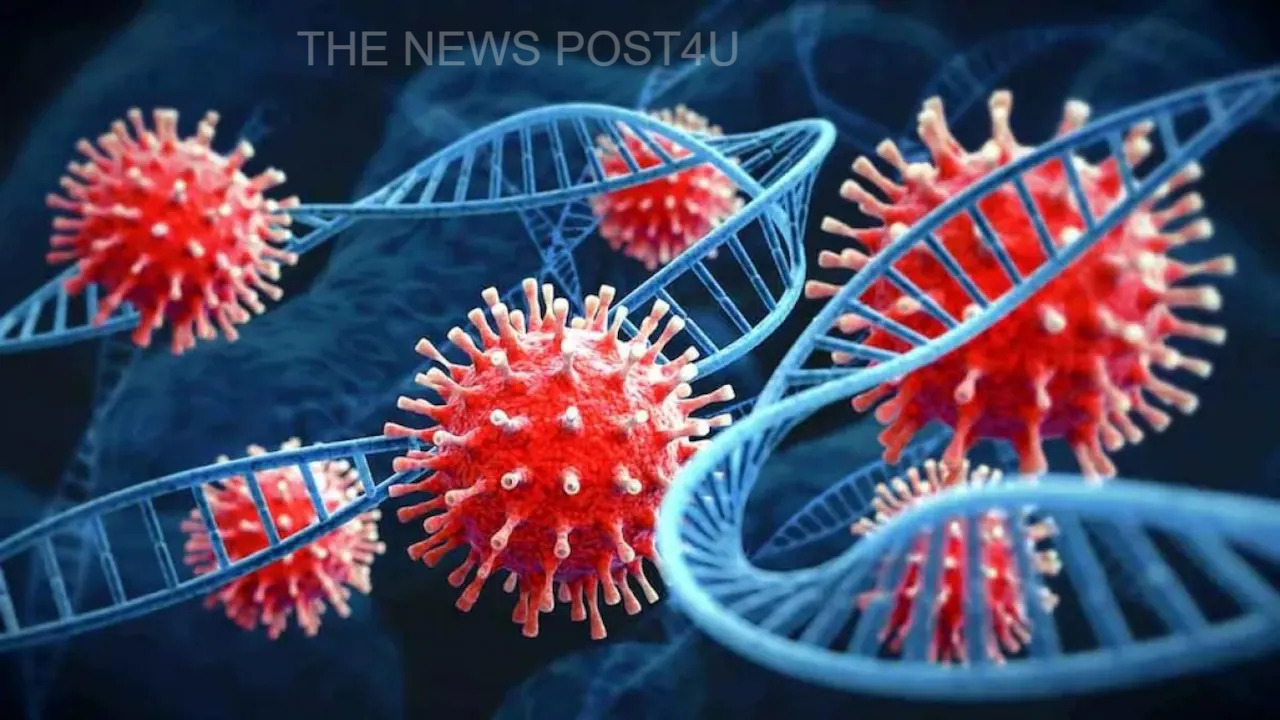By- Perwez Alam
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट का ताज़ा आदेश एक बार फिर उस बहस को सामने लेकर आया है, जो भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे के मूल में छिपी है। सुप्रीम कोर्ट ने उपासना स्थल अधिनियम, 1991 के तहत मस्जिदों या किसी अन्य धार्मिक स्थल पर नए दावे दाखिल करने पर रोक लगा दी है। यह रोक तब तक जारी रहेगी जब तक अदालत इस कानून की वैधता पर फैसला नहीं सुना देती।
यह अधिनियम 15 अगस्त, 1947 की स्थिति को बनाए रखने की बात करता है, और धार्मिक स्थलों के स्वरूप में किसी भी बदलाव या दावों पर रोक लगाता है। मगर सवाल यह है—क्या यह कानून सभी को समान रूप से न्याय दे पा रहा है? या यह अतीत के घावों को भरने के बजाय उन्हें और कुरेदने का कारण बन रहा है?
फैसले का राजनीतिक और कानूनी प्रभाव
प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन बेंच ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक इस कानून पर सुनवाई पूरी नहीं होती, कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं होगा। लेकिन अदालत ने यह भी कहा कि लंबित मामलों में कोई अंतिम फैसला भी फिलहाल नहीं दिया जाएगा।
वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले से लेकर मथुरा के शाही ईदगाह विवाद तक, कई मामले इस अधिनियम की छाया में हैं। इन मुकदमों का दावा है कि इन मस्जिदों का निर्माण प्राचीन मंदिरों को तोड़कर किया गया था। लेकिन क्या इस तरह के मुकदमे एक नई न्यायिक परंपरा की मांग कर रहे हैं, या यह समाज को विखंडित करने वाली राजनीति का हिस्सा हैं?
सवाल जो अदालत से परे हैं
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और अन्य राजनीतिक समूह इस कानून को देश की एकता और धर्मनिरपेक्षता के लिए आवश्यक मानते हैं। लेकिन याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह अधिनियम न्याय पाने के मूल अधिकार को छीनता है।
राजनीति इस मामले में गहराई तक जुड़ी हुई है। सुब्रमण्यम स्वामी जैसे नेता जहां इसे हिंदू धर्म के साथ न्याय करने का अवसर मानते हैं, वहीं मुस्लिम पक्ष इसे अपनी धार्मिक आजादी और सामाजिक शांति के लिए महत्वपूर्ण मानता है।
क्या वाकई शांति का मार्ग प्रशस्त होगा?
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से फिलहाल विवादों पर विराम लगा है, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं है। सवाल यह है कि क्या हमारा समाज बीते समय की गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़ेगा, या इन गलतियों को दोहराकर वर्तमान को और जटिल बनाएगा?
यह देखना दिलचस्प होगा कि जब अदालत इस कानून पर अंतिम निर्णय देगी, तो वह केवल कानूनी पहलू को ध्यान में रखेगी या सामाजिक-सांस्कृतिक और राजनीतिक नतीजों का भी आकलन करेगी।
जैसा कि एक पुरानी कहावत है—“न्याय में देरी करना, न्याय से इनकार करने के समान है।” लेकिन क्या इस न्याय की परिभाषा अब बदलनी चाहिए? यह जवाब अदालत के फैसले और समाज की प्रतिक्रिया में छिपा है।